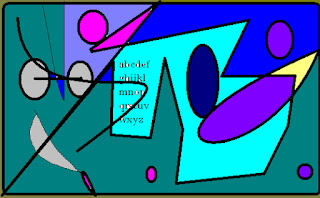बचपन
बचपन में क्रिकेट खेलने का शौक मुझे भी उतना ही था, जितना कि ज्यादातर हिंदुस्तानियों को होता है। रबर की गेंद और कपड़े धोेने-कूटने की ‘डमड़ी‘ (यह पंजाबी भाषा का शब्द है। इससे हिंदी साहित्य समृद्ध होगा। हर कूटने वाली चीज से हिंदी साहित्य समृद्ध होता है।) से अपने घरेलू आंगन में खेलते-खेलते हम मोहल्ले की पिच और काॅर्क की गंेद तक तरक्की कर गए।
बचपन में हम कहीं अधिक प्रगतिशील थे। सो महिला-पुरूष का भेद नहीं करते थे। लड़कियां मजे़ से हमारे साथ खेला करतीं। लड़कियांे के साथ तो मैं खेल लेता था, पर उनकी भावनाओं और इज़्ज़त आबरू के साथ खेलना नहीं जानता था। तब इतनी समझ नहीं थी। अब समझ आई है, तो हिम्मत साथ नहीं देती। जब हिम्मत साथ देती है, तो लड़कियां नहीं होतीं! खैर! जो लड़कियां उस वक्त तेज़ गेंदबाजी किया करती थीं या चैके छक्के लगाया करती थीं, वो आज अपने-अपने पतियों के यहां चैका बर्तन कर रही हैं। पति लोग ड्राइंग-रूम में सोफे पर बैठे टीवी पर मैच देख रहे हैं। बचपन की प्रगतिशीलता ने जवानी मेें परम्परा के आगे हथियार डाल दिए हैं।
मैं शुरू से ही आॅंल-राउंडर था। जैसी बैटिंग करता था, वैसी ही बाॅलिंग भी कर लेता था। खुलकर कहूं, तो न तो ढंग से गेंदबाजी कर पाता था न बल्लेबाजी। फलस्वरूप अधिकतर समय फील्डिंग ही करता रहता। धैर्य का अभाव मुझमें नहीं था। जब गेंद सीमा रेखा के बाहर जाकर अपने आप रूक जाती या कोई संभावित कैच धरती पर गिरकर शांत हो जाता, तब मैं गेंद उठाकर बीच में खड़े खिलाड़ियों की मार्फत बाॅलर या कप्तान तक पहुंचा देता।
अपवाद-स्वरूप कई दफा ऐसा भी होता कि हमारी टीम को जीतने के लिए दस-बारह रनों की जरूरत होती और आखिरी विकेट के रूप में मैं ही बचा होता। ऐसे मौकों पर अकसर यह होता कि मुझे गेंद फेंकने वाले तेज़ गंेदबाज के अपना रन-अप पूरा कर लेने से पहले ही मेरी माताजी मैदान में आ जातीं। वे हमारे कप्तान को डांट कर कहतीं कि क्या तुम्हारी जीत मेरे बच्चे की जिन्दगी से बड़ी है। इस पर सभी खिलाड़ी वक्ती तौर पर शर्मिंदा हो जाते। ममता, वात्सल्य और भावुकता के मिलेजुले भावों के साथ माता जी ज़बरदस्ती मुझे दर्शकों में बिठा देतीं। तेज़ गेंदबाज़ को अपनें बाॅलिंग-मार्क से राॅकेट की तरह छूटते देख, बुरी तरह घबराया, कंपकंपाया हुआ मैं मन ही मन माता जी को कई कई धन्यवाद देता, मगर ऊपर ऊपर कहता कि आज आपने रोक न लिया होता, तो मैं इन सालों की मिट्टी पलीत करके रख देता।
लेकिन यहीं से मेरे खेल जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। दर्शकों में बैठा हुआ मैं एक निष्कासित की तरह चिढ़ते हुए, खिलाड़ियों पर छींटाकशी करता। उनके खेल में मीनमेख निकालता। यह तो बाद में आकर पता चला कि इस छींटाकशी को कलमबद्ध करके कागज़ पर उतार दिया जाए, तो साहित्य में इसे कई बार व्यंग्य का दर्जा दिया जाता है।
बहरहाल, इस अध्याय की अगली पंक्तियों में हुआ यह कि धीरे-धीरे हमारे मोहल्ले के सभी खिलाड़ी खेलने के बजाय मैच को सुनने और देखने में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। इस मुकाम पर आकर मेरे और उनके बीच का फर्क खत्म हो गया। हम सब एक ही स्तर पर उतर आए। टीवी पर मैच देखते समय हम सब एक ही ढंग से चिल्लाते, हंसते, उछलते, तालियां पीटते या गालियां बकते। अब हमारी गणना देश के उन लोगों में होने लगी, जो मैच को खेलने के बजाय देखते हैं , मगर उस पर सट्टा आदि खेलते हैं।
फिर हमारे देखते-देखते पता नहीं कब यह हुआ कि टैस्ट मैचों को लगभग घूरे पर पटक दिया गया और उनकी जगह वन-डे मैचों की ताजपोशी कर दी गई। काफी कुछ बदला, मगर कुछ चीजें वैसे की वैसी रहीं। मसलन आज तक हमारे खिलाड़ी ठीक से तय नहीं कर पाए कि उन्हें जीतने के लिए खेलना चाहिए या खेलने के लिए जीतना चाहिए।
वैसे तो अपनी-अपनी तरह से सभी देश जीतने के लिए खेलते हैं। सभी खिलाड़ी भी जीतने के लिए यथासंभव योगदान देते हैं। मैं अकसर टी।वी। पर देखता हूं कि जब भारत दो जमे हुए बल्लेबाजों में से एक के आउट हो जाने पर संकट में आ जाता है, तो नया बल्लेबाज़ आकर पहले जमे हुए बल्लेबाज़ के साथ विकेटों के बीच कुछ देर मंत्रणा करता है। मैं अकसर मान लेता हूं कि कप्तान ने कोई बढ़िया तरकीब सुझाता हुआ संदेश भेजा होगा और अब ये दोनों मिलकर भारत को संकट से निकाल लेंगे। मगर देखता क्या हूं कि अगले ही ओवर में जमा हुआ बल्लेबाज आउट हो जाता है। संकटपूर्ण मौकों पर जब भी ऐसा होता है, तो मुझे अपने बचपन की क्रिकेट याद आ जाती है। तब मुझे लगता है कि जरुर इस जमे हुए बल्लेबाज की माताजी ने संदेश भिजवाया होगा कि बेटा, जब हमारे सारे बल्लेबाज़ ही एक-एक करके ढेर होते जा रहे हैं तो तू ही इकला क्यों लगा पड़ा है। देश क्या तेरे इकले का है। मेहनत तू करे और खाएं सब! ये कोई बात है! भाड़-चूल्हे में जाने दे रनों को। मैं घर से तेरे लिए गरमागरम हलवा बनाकर लाई हूं। आ जा जल्दी-जल्दी । खा जा।
हम दर्शकों का मनोविज्ञान भी हार और जीत के साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि हमारा धांसू बल्लेबाज तेजप्रकाश बहुत बढ़िया खेल रहा है। अर्द्धशतक पूरा कर चुका है। शतक की ओर बढ़ रहा है। तभी एक तेज गेंद पर और भी तेजी से बैट घुमाता है, मगर लपक लिया जाता है। तेजप्रकाश आउट। अब पहली स्थिति देखिए, जबकि बाद में भारत मैच हार जाता हैः-
‘तेज प्रकाश वो शाॅट बिल्कुल गलत खेला।
‘‘ये तो हमेशा ही ऐसा करता है।
‘‘कम-से-कम शतक तो पूरा कल्लेता‘
‘उसे इस बाॅल को छूने की जरूरत ही क्या थी!?
‘‘क्यों? सीधी बाॅल थी। बोल्ड हो जाता तो।?
‘‘हो जाता तो हो जाता। पर ऐसे वक्त पर ऐसी बाॅल को छेड़ना बेवकूफी है।‘
‘हां यार! हमारी टीम ही फुसफसी है। तेज प्रकाश को तो अब टीम से निकाल ही देना चाहिए। अपने आप अक्ल ठिकाने आ जाएगी।‘
दूसरी स्थिति वह है, जब भारत इसी मैच को जीत जाता हैः-
‘मज़ा आ गया यार! कमाल कर दिया हमारी टीम ने।
‘‘मैं कहता था न हमारी टीम दुनिया की नंबर एक की ठीम है।
‘‘एक-एक खिलाड़ी ने ग़ज़ब के हाथ दिखाए। भुस भर के रख दिया।
‘‘तेज प्रकाश ने तो यार गजब कर दिया। अकेला ही उनकी पूरी टीम पर भारी पड़ गया।
‘‘पर यार, जिस शाॅट पर वो आउट हुआ, वो उसने थोड़ा ठीक नहीं खेला।
‘‘अरे छोड़ यार, वो तो गेंद बल्ले पर पूरी तरह आई नहीं, नहीं तो सीधा छक्का ही होता।‘
आखिर में एक कपोल-कल्पित किस्सा (आप चाहें, तो इसे हकीकत भी मान सकते हैं)ः एक फील्डर से एक आसान कैच छूट गया। बाद में उसकी टीम वो मैच भी हार गई। साथी खिलाड़ियों ने पूछा कि जब गेंद सीधी ही तेरे हाथ में आ रही थी, तो तूने गेंद की तरफ पीठ करके उसे कैच करने जैसी अजीबोगरीब हरकत क्यों की। फील्डर बोला कि अगर वो ऐसा न करता, तो उसका पचास हजार रूपये का नुकसान हो जाता। जिस प्रायोजक ने अपना विज्ञापन उसकी छाती पर छापा था, उसने करार किया था कि टीवी के पर्दे पर जितनी बार तेरी शर्ट के सामने वाले हिस्से पर छपा हमारा विज्ञापन दिखाई देगा, उतनी बार के हिसाब से हम तुझे पचास हजार रूपये (प्रति झलक) देंगे। कब से मैं टीवी कैमरा की ओर पीठ किए खड़ा था। इतने लंबे इंतजार के बाद यह गेंद आई और मुझे पचास हजार कमाने का मौका मिला। भाई लोग, कैच लपकने का मौका तो जिंदगी भर मिलता रहेगा, मगर ये पचास हजार मैं अपने हाथ से कैसे स्लिप हो जाने देता। इस तरह व्यवसायिकता क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है।
-संजय ग्रोवर
(3 जुलाई, 1998 को अमर उजाला में प्रकाशित)